Discover श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप
श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप
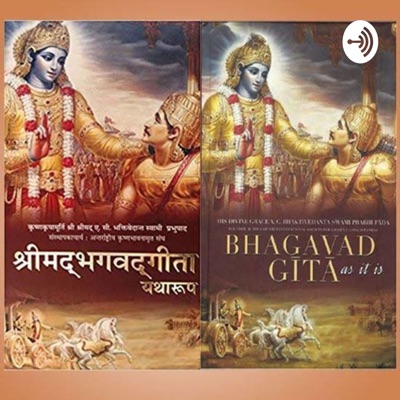
128 Episodes
Reverse
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते |
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति || ५ ||
यत्– जो; सांख्यैः - सांख्य दर्शन के द्वारा; प्राप्यते– प्राप्त किया जाता है; स्थानम्– स्थान; तत्– वही; योगैः– भक्ति द्वारा; अपि– भी; गम्यते– प्राप्त कर सकता है; एकम्– एक; सांख्यम्– विश्लेषात्मक अध्ययन को; च– तथा; योगम्– भक्तिमय कर्म को; च– तथा; यः– जो; पश्यति– देखता है; सः– वह; पश्यति– वास्तव में देखता है |
जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन (सांख्य) द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्ययोग तथा भक्तियोग को एकसमान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप मेंदेखता है |
तात्पर्य : दार्शनिक शोध (सांख्य) का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरमलक्ष्य की खोज है | चूँकि जीवन का चरमलक्ष्य आत्म-साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अन्तर नहीं है | सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि जीव भौतिक जगत् का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है | फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत् से कोई सराकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्र्वर से सम्बद्ध होने चाहिए | जब वह कृष्णभावनामृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है | सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्तियोग में उसे कृष्णभावनाभावित कर्म में आसक्त होना होता है | वस्तुतः दोनों ही विधियाँ एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दीखती है और दूसरे में आसक्ति है | जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है |
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः |
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् || ४ ||
सांख्य– भौतिक जगत् का विश्लेषात्मक अध्ययन; योगौ– भक्तिपूर्ण कर्म, कर्मयोग; पृथक्– भिन्न; बालाः– अल्पज्ञ; प्रवदन्ति– कहते हैं; न– कभी नहीं; पण्डिताः– विद्वान जन; एकम्– एक में; अपि– भी; आस्थितः– स्थित; सम्यक्– पूर्णतया; उभयोः– दोनों को; विन्दते– भोग करता है; फलम्– फल |
अज्ञानी ही भक्ति (कर्मयोग) को भौतिक जगत् के विश्लेषात्मक अध्ययन (सांख्य) से भिन्न कहते हैं | जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभाँति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है |
तात्पर्य : भौतिक जगत् के विश्लेषात्मक अध्ययन (सांख्य) का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है | भौतिक जगत् की आत्मा विष्णु या परमात्मा हैं | भगवान् की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है | एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है | सांख्यदर्शन का वास्तविक छात्र जगत् के मूल अर्थात् विष्णु को ढूँढता है और फिर पूर्णज्ञान समेत अपने को भगवान् की सेवा में लगा देता है | अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है | जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं हैं, किन्तु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है |
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति |
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते || ३ ||
ज्ञेयः– जानना चाहिए; सः– वह; नित्य - सदैव; संन्यासी– संन्यासी; यः– जो; न– कभी नहीं; द्वेष्टि– घृणा करता है; न– न तो; काङ्क्षति– इच्छा करता है; निर्द्वन्द्वः– समस्त द्वैतताओं से मुक्त; हि– निश्चय ही; महाबाहो– हे बलिष्ट भुजाओं वाले; सुखम्– सुखपूर्वक; बन्धात्– बन्धन से; प्रमुच्यते– पूर्णतया मुक्त हो जाता है |
जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य संन्यासी जाना जाता है | हे महाबाहु अर्जुन! ऐसा मनुष्य समस्त द्वन्द्वों से रहित होकर भवबन्धन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है |
तात्पर्य : पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुष नित्य संन्यासी है क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांशा करता है | ऐसा संन्यासी, भगवान् की दिव्य प्रेमभक्ति के परायण होकर पूर्णज्ञानी होता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है | वह भलीभाँति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण (अंशी) है और वह स्वयं अंशमात्र है | ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है | कृष्ण-तादात्मय की भावना भ्रान्त है क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता | यह ज्ञान कि एकता गुणों की है न कि गुणों की मात्रा की, सही दिव्यज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक | उसके मन में किसी प्रकार का छल-कपट नहीं रहता क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है | इस प्रकार छल-कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत् से भी मुक्त हो जाता है |
श्रीभगवानुवाच
संन्यासः कर्मयोगश्र्च निःश्रेयसकरावुभौ |
तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते || २ ||
श्री-भगवान् उवाच– श्रीभगवान् ने कहा; संन्यास– कर्म का परित्याग; कर्मयोगः– निष्ठायुक्त कर्म; च– भी; निःश्रेयस-करौ– मुक्तिपथ को ले जाने वाले; उभौ– दोनों; तयोः– दोनों में से; तु– लेकिन; कर्म-संन्यासात्– सकामकर्मों के त्याग से; कर्म-योगः – निष्ठायुक्त कर्म;विशिष्यते– श्रेष्ठ है |
श्रीभगवान् ने उत्तर दिया – मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय-कर्म (कर्मयोग) दोनों ही उत्तम हैं | किन्तु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है |
तात्पर्य:सकाम कर्म (इन्द्रियतृप्ति में लगाना) ही भवबन्धन का कारण है | जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहान्तरण करते हुए भवबन्धन को बनाये रखता है | इसकी पुष्टि भागवत (५.५.४-६) में इस प्रकार हुई है-
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति |
न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयमसन्नपि क्लेशद आस देहः ||
पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् |
यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः ||
एवं मनः कर्मवशं प्रयुंक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने |
प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् ||
“लोग इन्द्रियतृप्ति के पीछे मत्त हैं | वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम-कर्मों का फल है | यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किन्तु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है | अतः इन्द्रियतृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है | जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है | और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इन्द्रियतृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इन्द्रियतृप्ति की इस चेतना में फँसा रहता है तब तक उसका देहान्तरण होता रहता है | भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किन्तु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए | केवल तभी वह भव बन्धन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है |”
अतः यह ज्ञान ही (कि वह आत्मा है शरीर नहीं) मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं | जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा अन्यथा भवबन्धन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है | किन्तु कृष्णभावनाभावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है | पूर्णज्ञान से युक्त होकर किये गये कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं | बिना कृष्णभावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता | जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा | परन्तु कृष्णभावनाभावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसके उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता | अतः कृष्णभावनाभावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की सम्भावना बनी रहती है | कृष्णभावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृतसिन्धुमें (१.२.२५८) पुष्टि की है –
प्रापञ्चिकतया बुद्धया हरि समबन्धिवस्तुनः |
मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते ||
“जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्रीभगवान् से सम्बन्धित वस्तुओं को भौतिक समझ कर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है |” संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो की संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान् की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता | वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है | तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है? तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी सम्पत्ति कृष्ण की है, वह नित्य संन्यासी है | प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए | कृष्णभावनाभावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी संन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है |
अर्जुन उवाच
सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि |
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्र्चितम् || १ ||
अर्जुनः उवाच– अर्जुन ने कहा; संन्यासम्– संन्यास; कर्मणाम्– सम्पूर्ण कर्मों के; कृष्ण– हे कृष्ण; पुनः– फिर; योगम्– भक्ति; च – भी;शंससि– प्रशंसा करते हो; यत्– जो; श्रेयः– अधिक लाभप्रद है; एतयोः– इन दोनों में से; एकम्– एक; तत्– वह; मे– मेरे लिए;ब्रूहि– कहिये; सु-निश्चितम्– निश्चित रूप से |
अर्जुन ने कहा – हे कृष्ण! पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं | क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएँगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है?
तात्पर्य :भगवद्गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान् बताते हैं कि भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिन्तन से श्रेष्ठ है | भक्ति-पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्यस्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्मबन्धन से मुक्त करती है | द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बन्धन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है | उसी में बुद्धियोग अर्थात् भक्ति द्वारा इस भौतिक बन्धन से निकलने का भी वर्णन हुआ है | तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते | चतुर्थ अध्याय में भगवान् ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किन्तु चतुर्थ अध्याय के अन्त में भगवान् ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्णज्ञान से युक्त होकर, उठ करके युद्ध करे | अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त-अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है | अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है – इन्द्रियकार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग | किन्तु यदि भक्तियोग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ ? दूसरे शब्दों में, वह यह सोचता है कि ज्ञानमाय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं | ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बन्धनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है | अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्णज्ञान से युक्त होकर कर्म करे ?
तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः |
छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत || ४२ ||
तस्मात्– अतः; अज्ञान-सम्भूतम्– अज्ञान से उत्पन्न; हृत्स्थम्– हृदय में स्थित; ज्ञान– ज्ञान रूपी; असिना– शस्त्र से; आत्मनः– स्व के; छित्त्वा– काट कर; एनम्– इस; संशयम्– संशय को; योगम्– योग में; अतिष्ठ– स्थित होओ; उत्तिष्ठ– युद्ध करने के लिए उठो; भारत– हे भरतवंशी |
अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञानरूपी शस्त्र से काट डालो | हे भारत! तुम योग से समन्वित होकर खड़े होओ और युद्ध करो |
तात्पर्य : इस अध्याय में जिस योगपद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है | इस योग में दो तरह के यज्ञकर्म किये जाते है – एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है | यदि आत्म-साक्षात्कार के लिए द्रव्ययज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है | किन्तु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्णयज्ञ होता है | आध्यात्मिक क्रियाएँ भी दो प्रकार की होती हैं – आत्मबोध (या अपने स्वरूप को समझना) तथा श्रीभगवान् विषयक सत्य | जो भगवद्गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है | उसके लिए भगवान् के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है | ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान् के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है | इस अध्याय के प्रारम्भ में स्वयं भगवान् ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है | जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है और जो भगवान् द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान् के सच्चिदानन्द स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है | कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है | यह कृष्णभावनामृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इन्द्रियसंयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्ययज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रमधर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है | ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं | किन्तु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्त्वपूर्ण कारक आत्म-साक्षात्कार है | जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद्गीता का वास्तविक पाठक है, किन्तु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है | अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद्गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे | प्रामाणिक गुरु अनन्तकाल से चली आने वाली परम्परा में होता है और वह परमेश्र्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद्गीता के उपदेश इस धराधाम में आये | अतः गीता में ही व्यक्त भगवद्गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म-श्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं | भगवान् निश्चित रूप से परमपुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं | जो इसे समझता है वह भगवद्गीता का अध्ययन शुभारम्भ करते ही मुक्त होता है |
इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय “दिव्य ज्ञान” का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ |
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् |
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय || ४१ ||
योग– कर्मयोग में भक्ति से; संन्यस्त– जिसने त्याग दिये हैं; कर्माणम्– कर्मफलों को; ज्ञान– ज्ञान से; सञ्छिन्न– काट दिये हैं; संशयम्– सन्देह को; आत्म-वन्तम्– आत्मपरायण को; न– कभी नहीं; कर्माणि– कर्म; निब्ध्नन्ति– बाँधते हैं; धनञ्जय– हे सम्पत्ति के विजेता |
जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्यज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है | हे धनञ्जय! वह कर्मों के बन्धन से नहीं बँधता |
तात्पर्य : जो मनुष्य भगवद्गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान् श्रीकृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्यज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है | पूर्णतः कृष्णभावनाभावित होने के कारण उसे श्रीभगवान् के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है | अतएव निस्सन्देह वह कर्मबन्धन से मुक्त है |
अज्ञश्र्चाश्रद्दधानश्र्च संशयात्मा विनश्यति |
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः || ४० ||
अज्ञः– मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है; च– तथा; अश्रद्दधानः– शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन; च– भी; संशय– शंकाग्रस्त; आत्मा– व्यक्ति; विनश्यति– गिर जाता है; न– न; अयम्– इस; लोकः– जगत में; अस्ति– है; न– न तो; परः– अगले जीवन में; न– नहीं; सुखम्– सुख; संशय– संशयग्रस्त; आत्मनः– व्यक्ति के लिए;
किन्तु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवद्भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते है | संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में, न ही परलोक में कोई सुख है |
तात्पर्य :भगवद्गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है | जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किन्तु उनमें वास्तविक विश्र्वास नहीं करते | यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद्गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी वे न तो भगवान् कृष्ण में विश्र्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं | ऐसे लोगों को कृष्णभावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता | वे नीचे गिरते हैं | उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते | जो लोग ईश्र्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में न तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है | उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है | अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धाभाव से शास्त्रों के सिद्धान्तों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे | इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुँच सकता है | दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता | अतः मनुष्य को चाहिए कि परम्परा से चले आ रहे महान आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे |
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन |
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा || ३७ ||
यथा - जिस प्रकार से; एधांसि - ईंधन को; समिद्धः - जलती हुई; अग्निः - अग्नि; भस्म-सात् - राख; कुरुते - कर देती है; अर्जुन - हे अर्जुन; ज्ञान-अग्निः - ज्ञान रूपी अग्नि; सर्व-कर्माणि - भौतिक कर्मों के समस्त फल को; भस्मसात् - भस्म, राख; कुरुते - करती है; तथा - उसी प्रकार से |
जैसे प्रज्ज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन! ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है ।
तात्पर्य : आत्मा तथा परमात्मा सम्बन्धी पूर्णज्ञान तथा उनके सम्बन्ध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है । यह अग्नि न केवल समस्त पापकर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्यकर्मों के फलों को भी भस्मसात् करने वाली है । कर्मफल की कई अवस्थाएँ हैं - शुभारम्भ, बीज, संचित आदि । किन्तु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती । वेदों में (बृहदारण्यक उपनिषद् ४.४.२२) कहा गया है - उभे उहैवैष एते तरत्यमृतः साध्वासाधूनी - 'मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है ।'
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः |
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि || ३६ ||
अपि - भी; चेत् - यदि; असि - तुम हो; पापेभ्यः - पापियों से;सर्वेभ्यः - समस्त; पाप-कृत-तमः - सर्वाधिक पापी; सर्वम् - ऐसे समस्त पापकर्म; ज्ञान-प्लवेन - दिव्यज्ञान की नाव द्वारा; एव - निश्चय ही; वृजिनम् - दुखों के सागर को ; सन्तरिष्यसि - पूर्णतया पार कर जाओगे ।
यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाये तो भी तुम दिव्यज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख-सागर को पार करने में समर्थ होगे ।
तात्पर्य : श्री कृष्ण के सम्बन्ध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही-सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान-सागर में चलने वाले जीवन-संघर्ष से मनुष्य तुरन्त ही ऊपर उठ सकता है । यह भौतिक जगत् कभी-कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल । सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन-संघर्ष अत्यन्त कठिन है । यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है । भगवान् से प्राप्त पूर्णज्ञान मुक्ति का पथ है । कृष्णभावनामृत की नाव अत्यन्त सुगम है, किन्तु उसी के साथ-साथ अत्यन्त उदात्त भी ।
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव |
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि || ३५ ||
यत्– जिसे; ज्ञात्वा– जानकर; न– कभी नहीं; पुनः– फिर; मोहम्– मोह को; एवम्– इस प्रकार; यास्यसि– प्राप्त होगे; पाण्डव– हे पाण्डवपुत्र; येन– जिससे; भूतानि– जीवों को; अशेषेण– समस्त; द्रक्ष्यसि– देखोगे; आत्मनि– परमात्मा में; अथ उ– अथवा अन्य शब्दों में; मयि– मुझमें |
स्वरुपसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंशस्वरूप हैं, अर्थात् वे सब मेरे हैं |
तात्पर्य : स्वरुपसिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान् श्रीकृष्ण के भिन्न अंश हैं | कृष्ण से पृथक् अस्तित्व का भाव माया (मा – नहीं, या – यह) कहलाती है | कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है | वस्तुतः जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है | कृष्ण भगवान् के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण हैं | ब्रह्मसंहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्रीभगवान् हैं और सभी कारणों के कारण हैं | यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं | इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश हैं | मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक् अस्तित्व को मिटा देते हैं | यह विचार सर्वथा भौतिक है | भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखण्डन किया जाय तो उसका मूलस्वरूप नष्ट हो जाता है | किन्तु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है | परब्रह्म का यही स्वरूप है |
ब्रह्मविद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक् सोचते हैं | यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, किन्तु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं | जीवों का शारीरिक अन्तर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है | हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं | केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक सम्बन्ध कृष्ण के शाश्र्वत आध्यात्मिक सम्बन्धों से अधिक महत्त्वपूर्ण है | गीता का सम्पूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक् नहीं हो सकता, कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है | परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है | उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं | ऐसे शारीरिक अन्तर भगवान् के दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं | किन्तु जब कोई कृष्णभावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरन्त मुक्त हो जाता है | ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है | पूर्णज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक् समझते हैं | इस तरह विभिन्न भौतिक पहिचानों के मानदण्डों के अन्तर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं | किन्तु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्णभावनामृत में स्थित होते हैं तो यहसमझा जाता है कि वे मुक्ति-पथ पर हैं जिसकी पुष्टि भागवत में (२.१०.६) की गई है – मुक्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः| मुक्ति का अर्थ है – कृष्ण के नित्य दास रूप में (कृष्णभावनामृत में) अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना |
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया |
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः || ३४ ||
तत्– विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को; विद्धि– जानने का प्रयास करो; प्रणिपातेन– गुरु के पास जाकर के; परिप्रश्नेन– विनीत जिज्ञासा से; सेवया– सेवा के द्वारा; उपदेक्ष्यन्ति– दीक्षित करेंगे; ते– तुमको; ज्ञानम्– ज्ञान में; ज्ञानिनः– स्वरुपसिद्ध; तत्त्व– तत्त्व के; दर्शिनः– दर्शी |
तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो | उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो | स्वरुपसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है |
तात्पर्य : निस्सन्देह आत्म-साक्षात्कार का मार्ग कठिन है अतः भगवान् का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारम्भ होने वाली परम्परा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए | इस परम्परा के सिद्धान्त का पालन किये बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता | भगवान् आदि गुरु हैं, अतः गुरु-परम्परा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान् का सन्देश प्रदान कर सकता है | कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरुपसिद्ध नहीं बन सकता जैसा कि आजकल के मुर्ख पाखंडी करने लगे हैं | भागवत का (६.३.१९) कथन है – धर्मंतुसाक्षात्भगत्प्रणीतम – धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान् ने किया है | अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता | न ही ज्ञानग्रंथों के स्वतन्त्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है | ज्ञान-प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा | ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकाररहित होकर दास की भाँति गुरु की सेवा करनी चाहिए | स्वरुपसिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है | जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है | बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएँ प्रभावपूर्ण नहीं होंगी | शिष्य को गुरु-परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है | इस श्लोक में अन्धानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा-इन दोनों की भर्त्सना की गई है | शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे | प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है |
श्रेयान्द्रव्यमयाद् यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप |
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते || ३३ ||
श्रेयान्– श्रेष्ठ; द्रव्य-मयात्– सम्पत्ति के; यज्ञात्– यज्ञ से; ज्ञान-यज्ञः– ज्ञानयज्ञ; परन्तप– हे शत्रुओं को दण्डित करने वाले; सर्वम्– सभी; कर्म– कर्म; अखिलम्– पूर्णतः; पार्थ– हे पृथापुत्र; ज्ञाने– ज्ञान में; परिसमाप्यते– समाप्त होते हैं |
हे परंतप! द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है | हे पार्थ! अन्ततोगत्वा सारे कर्मयज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते है |
तात्पर्य : समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्णज्ञान प्राप्त हो जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अन्त में परमेश्र्वर की दिव्य सेवा कर सके | तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए | कभी-कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते है | जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्यज्ञान के स्तर तक पहुँच जाती है तो उसे ज्ञानरहित द्रव्ययज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता | यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्णभावनामृत में होता है जो दिव्यज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है | ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है | किन्तु जब उसे दिव्यज्ञान के स्तर तक पहुँचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं | चेतनाभेद के अनुसार ऐसे यज्ञकर्म कभी-कभी कर्मकाण्ड कहलाते हैं और कभी ज्ञानकाण्ड | यज्ञ वही श्रेष्ठ है, जिसका अन्त ज्ञान में हो |
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे |
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे || ३२ ||
एवम्– इस प्रकार; बहु-विधाः– विविध प्रकार के; यज्ञाः– यज्ञ; वितताः– फैले हुए हैं; ब्रह्मणः– वेदों के; मुखे– मुख में; कर्म-जान्– कर्म से उत्पन्न; विद्धि– जानो; तान्– उन; सर्वान्– सबको; एवम्– इस तरह; ज्ञात्वा– जानकर; विमोक्ष्यसे– मुक्त हो जाओगे |
ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदसम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं | इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे |
तात्पर्य : जैसा कि पहले बताया जा चुका है वेदों में कर्ताभेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है | चूँकि लोग देहात्मबुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार सम्पन्न कर सके | किन्तु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सबका विधान है | इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान् ने अपने श्रीमुख से की है |
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम || ३१ ||
न– कभी नहीं; अयम्– यह; लोकः– लोक; अस्ति– है; अयज्ञस्य– यज्ञ न करने वाले का; कुतः– कहाँ है; अन्यः- अन्य; कुरु-सत्-तम– हे कुरुश्रेष्ठ |
हे कुरुश्रेष्ठ! जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा?
तात्पर्य : मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है | दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत् में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है | अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत् में अस्तित्व का कारण है | मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बन्धन से बाहर निकला जा सकता है | अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बहार निकालने का अवसर प्रदान करते हैं | धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं | जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ सम्पन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है | जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है, तो इन्द्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है | अतः वेदों में नियमित इन्द्रियतृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है | इस प्रकार मनुष्य भौतिक बन्धन से क्रमशः छूटकर उच्चपद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्र्वर का सान्निध्य प्राप्त करने में है | यह पूर्णता यज्ञ सम्पन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है | फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है | विभिन्न स्वर्गों में भिन्न-भिन्न प्रकार की जीवन-सुविधाएँ हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है | किन्तु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्णभावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुण्ठ जाकर प्राप्त करता है | अतः कृष्णभावनाभावित जीवन ही इस भौतिक जगत् की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है |
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे |
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्र्च यतयः संशितव्रताः || २८ ||
द्रव्य-यज्ञाः– अपनी सम्पत्ति का यज्ञ; तपः-यज्ञाः– तपों का यज्ञ; योग-यज्ञाः– अष्टांग योग में यज्ञ; तथा– इस प्रकार; अपरे– अन्य; स्वाध्याय– वेदाध्ययन रूपी यज्ञ; ज्ञान-यज्ञाः– दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ; च– भी; यतयः– प्रबुद्ध पुरुष; संशित-व्रताः– दृढ व्रतधारी |
कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी सम्पत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योगपद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्यज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं |
तात्पर्य : इन यज्ञों के कई वर्ग किये जा सकते हैं | बहुत से लोग विविध प्रकार के दान-पुण्य द्वारा अपनी सम्पत्ति का यजन करते हैं | भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएँ खोल देते हैं – यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ | अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएँ प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं | ये सब दानकर्म द्रव्यमययज्ञ हैं | अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च्लोकों में जाने के लिए चान्द्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं | इन विधियों के अन्तर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं | उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के चार मासों (जुलाई से अक्टूबर तक) बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएँ खाता है और न दिन में दो बार खाता है, न निवास-स्थान छोड़कर कहीं जाता है | जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमययज्ञ कहलाता है | कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योगपद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति (ब्रह्म में तदाकार होने के लिए) अथवा हठयोग या अष्टांगयोग (विशेष सिद्धियों के लिए) | कुछ लोग समस्त तीर्थस्थानों की यात्रा करते हैं | ये सारे अनुष्ठान योग-यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत् में किसी सिद्धि विशेष के लिए किये जाते हैं | कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद् तथा वेदान्तसूत्र या सांख्यादर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं | इसे स्वाध्याययज्ञ कहा जाता है | ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्चजीवन की तलाश में रहते हैं | किन्तु कृष्णभावनामृत इनसे पृथक् है क्योंकि यह परमेश्र्वर की प्रत्यक्ष सेवा है | इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान् तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है | फलतः कृष्णभावनामृत दिव्य है |
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे |
आत्मसंयमयोगग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते || २७ ||
सर्वाणि– सारी; इन्द्रिय– इन्द्रियों के; कर्माणि– कर्म; प्राण-कर्माणि– प्राणवायु के कार्यों को; च– भी; अपरे– अन्य; आत्म-संयम– मनोनिग्रह को; योग– संयोजन विधि; अग्नौ– अग्नि में; जुह्वति– अर्पित करते हैं, ज्ञान-दीपिते– आत्म-साक्षात्कार की लालसा के कारण |
दूसरे, जो मन तथा इन्द्रियों को वश में करके आत्म-साक्षात्कार करना चाहते हैं, सम्पूर्ण इन्द्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं |
तात्पर्य : यहाँ पर पतञ्जलि द्वारा सूत्रबद्ध योगपद्धति का निर्देश है | पतंजलि कृत योगसूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है | जब तक जीवात्मा इन्द्रियभोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है और ज्योंही वह इन्द्रियभोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है | जीवात्मा के शरीर में दस प्रकार के वार्यु कार्यशील रहते हैं और इसे श्र्वासप्रक्रिया (प्राणायाम) द्वारा जाना जाता है | पतंजलि की योगपद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियन्त्रित किया जाए जिससे अन्ततः वायु के सभी आन्तरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएँ | इस योगपद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है | यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है | इन्द्रियाँ इन्द्रियविषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूँघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं, और ये सब इन्द्रियाँ मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं | ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार (क्रियाएँ) हैं | अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्मा-साक्षात्कार की खोज में लगाता है |
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति |
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति || २६ ||
श्रोत्र-आदीनि– श्रोत्र आदि; इन्द्रियाणि– इन्द्रियाँ; अन्ये– अन्य; संयम– संयम की; अग्निषु– अग्नि में; जुह्वति– अर्पित करते हैं; शब्द-आदीन्– शब्द आदि; विषयान्– इन्द्रियतृप्ति के विषयों को; अन्ये– दूसरे; इन्द्रिय– इन्द्रियों की; अग्निषु– अग्नि में; जुह्वति– यजन करते हैं |
इनमें से कुछ (विशुद्ध ब्रह्मचारी) श्रवणादि क्रियाओं तथा इन्द्रियों को मन की नियन्त्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं तो दूसरे लोग (नियमित गृहस्थ) इन्द्रियविषयों को इन्द्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं |
तात्पर्य : मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य – ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी-पूर्णयोगी बनने के निमित्त हैं | मानव जीवन पशुओं की भाँति इन्द्रियतृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके | ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इन्द्रियतृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं | वे कृष्णभावनामृत से सम्बन्धित शब्दों को ही सुनते हैं | श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर्नामानुकीर्तनम् अर्थात् भगवान् के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है | वह सांसारिक शब्द-ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है | इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इन्द्रियतृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं | यौन जीवन, मादकद्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं, किन्तु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इन्द्रियतृप्ति के कार्यों में अनियन्त्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता | इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म-विवाह का प्रचलन है | यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इन्द्रियतृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है |
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते |
ब्रह्मग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति || २५ ||
दैवम्– देवताओं की पूजा करने में; एव– इस प्रकार; अपरे– अन्य; यज्ञम्– यज्ञ को; योगिनः– योगीजन; पर्युपासते– भलीभाँति पूजा करते हैं; ब्रह्म– परमसत्य का; अग्नौ – अग्नि में; अपरे– अन्य; यज्ञम्– यज्ञ को; यज्ञेन– यज्ञ से; एव– इस प्रकार; उपजुह्वति– अर्पित करते हैं |
कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभाँति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं |
तात्पर्य : जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्णभावनाभावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है, किन्तु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं | इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं | विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा सम्पन्न यज्ञ की ये कोटियाँ केवल बाह्य वर्गीकरण हैं | वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है – भगवान् विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं | विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है | सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ (द्रव्ययज्ञ) तथा दिव्य ज्ञान के लिए किये गये यज्ञ (ज्ञानयज्ञ) | जो कृष्णभावनाभावित हैं उनकी सारी भौतिक सम्पदा परमेश्र्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किन्तु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इन्द्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक सम्पदा की आहुति देते हैं | किन्तु अन्य लोग, जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं | देवतागण ऐसी शक्तिमान् जीवात्माएँ हैं जिन्हें ब्रह्माण्ड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्र्वर ने नियुक्त किया है | जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं | ऐसे लोग बह्वीश्र्वरवादी कहलाते हैं | किन्तु जो लोग परम सत्य निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्मकी अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं | ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्र्वर की दिव्यप्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिन्तन में अपना सारा समय लगाते हैं | दुसरे शब्दों में, सकामकर्मी भौतिकसुख के लिए अपनी भौतिक सम्पत्ति का यजन करते हैं, किन्तु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं | निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है | किन्तु अर्जुन जैसा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है | इस तरह उसकी सारी भौतिक सम्पत्ति के साथ-साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है | वह परम योगी है, किन्तु उसका पृथक् स्वरूप नष्ट नहीं होता |
*श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप*
अध्याय ४ श्लोक संख्या २३
*गतसङगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः |*
*यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते || २३ ||*
गत-सङगस्य– प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त; मुक्तस्य– मुक्त पुरुष का; ज्ञान-अवस्थित– ब्रह्म में स्थित; चेतसः– जिसका ज्ञान; यज्ञाय– यज्ञ (कृष्ण) के लिए; आचरतः– करते हुए; कर्म– कर्म; समग्रम्– सम्पूर्ण; प्रविलीयते– पूर्वरूप से विलीन हो जाता है |
*जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं |*
तात्पर्य : पूर्णरूपेण कृष्णभावनाभावित होने पर मनुष्य समस्त द्वन्द्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मष से भी मुक्त हो जाता है | वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्णभावनामृत से विचलित नहीं होता | अतएव वह जो कुछ भी करता है, वह आदिविष्णु कृष्ण के लिए होता है | अतः उसका सारा कर्म यज्ञरूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात् कृष्ण को प्रसन्न करना है | ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है |
🙏🏻🙏🏻🌹 *हरे कृष्णा* 🌹🙏🏻🙏🏻





