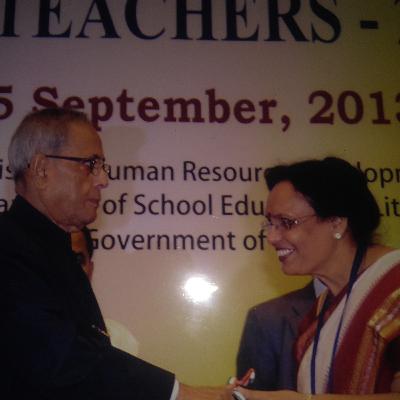Discover मधुरिम हिंदी
मधुरिम हिंदी

11 Episodes
Reverse
*21 अप्रैल,'सिविल सेवा दिवस'*
'सिविल सेवा' किसी भी देश के प्रशासनिक तंत्र की रीड की हड्डी मानी जाती है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में भी संविधान द्वारा निर्धारित कार्यकारी निर्णय इन सिविल सेवकों द्वारा ही कार्यान्वित किए जाते हैं।
आज ही के दिन, 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन करते हुए, भारतीय लोक सेवा के पहले दल को 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' के नाम से संबोधित किया था। स्वतंत्र भारत में सन 1950 से सिविल सेवाएं परीक्षाएं प्रारंभ हुई तथा 2006 से नियमित रूप से हर वर्ष 'सिविल सेवा दिवस' मनाया जाने लगा इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को नागरिकों के लिए समर्पित और वचनबद्ध कार्यों के लिए प्रेरित करना है। इन सिविल सेवकों के पास पारंपरिक और सांविधिक दायित्व भी होते हैं, जो कि कुछ हद तक सत्ता में किसी राजनीतिक पार्टी को अपनी राजनीतिक शक्ति का अनुचित लाभ उठाने एवं उसका निजी हित में इस्तेमाल करने से बचाता है। इस अवसर पर राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा उत्कृष्ट सिविल सेवा देने वाले अधिकारियों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाता है।
आज इस गौरवपूर्ण दिवस पर मैं आपको जीवट और संघर्ष की प्रतीक बन कर उभरी उस लौह महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो भारत की पहली आई.ए.एस. महिला थी। ...सुनेंगे?
...तो यह पॉडकास्ट आपके लिए ही है-
कहानी की तात्त्विक समीक्षा
प्रेमचंद के अनुसार "कहानी वह ध्रुपद की तान है, जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है, जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि "कहानी (गल्प) एक रचना है, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा-विन्यास, सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भाँति उसमें मानव-जीवन का संपूर्ण तथा वृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं, जिसमें भाँति-भाँति के फूल, बेल-बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है।’ इस प्रकार कहानी वह गद्य रचना है, जिसमें जीवन के किसी एक अंग का सर्वांग प्रस्तुतिकरण होता है।
कहानी के तत्त्व-
कहानी की रचना एक कलात्मक विधान है, जो अभ्यास और प्रतिभा के द्वारा रूपाकार ग्रहण करती है। रोचकता, प्रभाव तथा वक्ता एवं श्रोता या कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोचित सम्बद्धता बनाए रखने के लिए कहानियों में कथावस्तु, पात्र अथवा चरित्र-चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देशकाल अथवा वातावरण, भाषा-शैली तथा उद्देश्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व माने गए हैं-
कहानी के प्रमुख तत्त्व-
1. कथावस्तु –
कहानी के ढाँचे को कथानक अथवा कथावस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथावस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथावस्तु जीवन की भिन्न- मिन्न दिशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है- पुराण, इतिहास, राजनीतिक, समाज आदि। कहानीकार इनमे से किसी भी क्षेत्र से कथावस्तु का चुनाव करता है और उसके आधार पर कथानक की अट्टालिका खड़ी करता है।
कथावस्तु में घटनाओं की अधिकता हो सकती है और एक ही घटना पर उसकी रचना भी हो सकती है, लेकिन, उनमें कोई न कोई घटना अवश्य होगी। वैसे तो कथानक की पांच दशाएं होती है-आरंभ ,विकास ,कोतुहल ,चरमसीमा और अंत, परंतु प्रत्येक कहानी में पांचों अवस्थाएं नहीं होती।
(कहानी का नाम)"उसने कहा था" कहानी में कथानक संघर्ष की स्थिति को पार करता है , विकास को प्राप्त कर कौतूहल को जगाता हुआ , चरम सीमा पर पहुंचता है और उसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।
(कहानी का नाम ) "उसने कहा था" कथानक के चार अंग हैं - आरम्भ, आरोह, चरम स्थिति एवं अवरोह।
(कहानी की मुख्य घटनाएं).................…..................
(कहानी का नाम)"उसने कहा था" का कथा-विन्यास अत्यंत विराट फलक पर किया गया है। कहानी जीवन के किसी प्रसंग विशेष, समस्या विशेष या चरित्र की किसी एक विशेषता को ही प्रकाशित करती है, उसके संक्षिप्त कलेवर में इससे अधिक की गुंजाइश नहीं होती है, किंतु यह कहानी लहना सिंह के चारित्रिक विकास में उसकी अनेक विशेषताओं को प्रकाशित करती हुई उसका संपूर्ण जीवन-वृत्त प्रस्तुत करती है, बारह वर्ष की अवस्था से लेकर प्राय: सैंतीस वर्ष, उसकी मृत्यु तक की कथा-नायक का संपूर्ण जीवन इस रूप में चित्रित होता है कि कहानी अपनी परंपरागत रूप-पद्धति को चुनौती देकर एक महाकाव्यात्मक औदात्य लिये हुए है । वस्तुत: पांच खण्डों में कसावट से बुनी गयी यह कहानी सहज ही औपन्यासिक विस्तार से युक्त है किंतु अपनी कहन की कुशलता से कहानीकार इसे एक कहानी ही बनाये रखता है। दूसरे, तीसरे और चौखे खण्ड में विवेच्य कहानी में युद्ध कला, सैन्य-विज्ञान और खंदकों में सिपाहियों के रहने-सहने के ढंग का जितना प्रामाणिक, सूक्ष्म तथा जीवंत चित्रण इस कहानी में हुआ है, वैसा हिंदी कथा साहित्य में विरल है। मौलिकता,मौलिकता से तात्पर्य यहाँ नवीनता से है। सम्भाव्यता, सुगठितता एवं रोचकता चारों गुण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ‘संक्षिप्तता’ इस कहानी के कथानक का अनिवार्य गुण है। कहानी का आरम्भ, मध्य और अन्त सुगठित है,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कहानी के शरीर मेें कथानक हड्डियों के समान है, अतः (कहानीकार का नाम)ने कथानक की रचना अत्यन्त वैज्ञानिक तरीके से क्रमिक विकास के रूप में की है।
2. पात्र का चरित्र चित्रण –
कथावस्तु के बाद चरित्र-चित्रण कहानी का अत्यन्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। वस्तुतः पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से एक ओर कथानक का आरम्भ, विकास और अन्त होता है, तो दूसरी ओर हम कहानी में इनसे आत्मीयता प्राप्त करते हैं।
पात्रों के गुण-दोष को उनका 'चरित्र चित्रण' कहा जाता है। कहानी में वर्णित व्यक्ति ही कहानी में चरित्र कहलाता है।
कहानी का नाम) "उसने कहा था" कहानी में यथार्थवादी मनोविज्ञान पर बल दिया गया है अतः उसमें चरित्र चित्रण को अधिक
कहानी की तात्त्विक समीक्षा
प्रेमचंद के अनुसार "कहानी वह ध्रुपद की तान है, जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है, जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि "कहानी (गल्प) एक रचना है, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा-विन्यास, सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भाँति उसमें मानव-जीवन का संपूर्ण तथा वृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं, जिसमें भाँति-भाँति के फूल, बेल-बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है।’' इस प्रकार कहानी वह गद्य रचना है' जिसमें जीवन के किसी एक अंग का सर्वांग प्रस्तुतिकरण होता है।
कहानी के तत्त्व-
कहानी की रचना एक कलात्मक विधान है, जो अभ्यास और प्रतिभा के द्वारा रूपाकार ग्रहण करती है। रोचकता, प्रभाव तथा वक्ता एवं श्रोता या कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोचित सम्बद्धता बनाए रखने के लिए कहानियों में कथावस्तु, पात्र अथवा चरित्र-चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देशकाल अथवा वातावरण, भाषा-शैली तथा उद्देश्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व माने गए हैं-
कहानी के प्रमुख तत्त्व-
1. कथावस्तु –
कहानी के ढाँचे को कथानक अथवा कथावस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथावस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथावस्तु जीवन की भिन्न- मिन्न दिशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है- पुराण, इतिहास, राजनीतिक, समाज आदि। कहानीकार इनमें से किसी भी क्षेत्र से कथावस्तु का चुनाव करता है और उसके आधार पर कथानक की अट्टालिका खड़ी करता है।
कथावस्तु में घटनाओं की अधिकता हो सकती है और एक ही घटना पर भी कहानी की रचना हो सकती है लेकिन, उनमें कोई न कोई घटना अवश्य होगी। वैसे तो कथानक की पांच दशाएं होती है-आरंभ ,विकास ,कोतुहल ,चरमसीमा और अंत, परंतु प्रत्येक कहानी में पांचों अवस्थाएं नहीं होती।
(कहानी का नाम) कहानी में कथानक संघर्ष की स्थिति को पार करता है , विकास को प्राप्त कर कौतूहल को जगाता हुआ , चरम सीमा पर पहुंचता है और उसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।
इस .......(कहानी का नाम ) कथानक के चार अंग हैं - आरम्भ, आरोह, चरम स्थिति एवं अवरोह।
(कहानी की मुख्य घटनाएं).................…..................
(कहानी का नाम) कथानक में मौलिकता,मौलिकता से तात्पर्य यहाँ नवीनता से है। सम्भाव्यता, सुगठितता एवं रोचकता चारों गुण स्पष्ट रूप से दरखे जा सकते हैं। ‘संक्षिप्तता’ इस कहानी के कथानक का अनिवार्य गुण है। कहानी का आरम्भ, मध्य और अन्त सुगठित है,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी के शरीर मेें कथानक हड्डियों के समान है, अतः (कहानीकार का नाम)ने कथानक की रचना अत्यन्त वैज्ञानिक तरीके से क्रमिक विकास के रूप में की है।
2. पात्र एवं चरित्र चित्रण –
कथावस्तु के बाद चरित्र-चित्रण कहानी का अत्यन्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। वस्तुतः पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से एक ओर कथानक का आरम्भ, विकास और अन्त होता है, तो दूसरी ओर हम कहानी में इनसे आत्मीयता प्राप्त करते हैं।
पात्रों के गुण-दोष को उनका 'चरित्र चित्रण' कहा जाता है। कहानी में वर्णित व्यक्ति ही कहानी में चरित्र कहलाता है।
(कहानी का नाम)में पात्रों की संख्या सीमित है। (कहानीकार का नाम) पात्रों के बाह्य और अंतरिक पक्षों का अधिक से अधिक मनोविश्र्लेषण कर उन्हें मूल घटना के साथ गहराई से जोड़ देता है।
(कहानी का नाम) कहानी में यथार्थवादी मनोविज्ञान पर बल दिया गया है अतः उसमें चरित्र चित्रण को अधिक महत्त्व दिया गया है। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न कर घटना और कार्य व्यापार के स्थान पर पात्र और उसका संघर्ष को ही कहानी की मूल धुरी बना दिया है।
(कहानी के मुख्य पात्रों के नाम)
कहानी के छोटे आकार तथा तीव्र प्रभाव के कारण पात्रों की संख्या सीमित है। मुख्य पात्र के साथ साथ कहानी में दूसरे पात्र के सबसे अधिक प्रभाव पूर्ण पक्ष की उसके व्यक्तित्व की केवल सर्वाधिक पुष्ट तत्व की झलक ही प्रस्तुत की गई है। अतः कहानी के पात्र वास्तविक सजीव स्वाभाविक तथा विश्वसनीय लगते हैं। पात्रों का चरित्र आकलन (लेखक का नाम) ने दोनों प्रकार से किया है- प्रत्यक्ष या वर्णात्मक शैली द्वारा इसमें लेखक स्वयं पात्र के चरित्र में प्रकाश डालता हैऔर परोक्ष या नाट्य शैली में पात्र स्वयं अपने वार्तालाप और क्रियाकलापों द्वारा अपने गुण दोषों का संकेत देता चलता है।
इ
'कोणार्क' - जगदीश चंद्र माथुर
(एक विहंगम दृष्टि)-डॉ. मधुगुप्ता
'कोणार्क' जगदीश चन्द्र माथुर का एक प्रसिद्ध नाटक है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार "जगदीशचन्द्र माथुर का 'कोणार्क अत्यन्त सफल कृति है। नाट्यकला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि अन्यत्र देखने को नहीं मिली। विषय निर्वाचन, कथा-वस्तु, क्रम-विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्ययिता आदि दृष्टियों से कोणार्क अद्भुत कला-कृति है, जिसमें नाटक की सीमाएँ एक रहस्य विस्तार में खो-सी गई हैं। उपक्रम मेंमें आंखों के सामने एक विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंसशेप, कल्पना में समुद्र की तरह आरपार उद्वेलित होकर साकार हो उठता है, जिसकी तरंगों के व्यया-द्रवित उत्यान-पतन में करुण, विद्रोह-भरा नाटक का कयानक मन की आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाता है। उपसंहार में नाटक की अमर अमिट अनुगूंज हृदय के श्रवणों में अविराम गूंजती रहती हैं। इस नाटक का तृतीय अंक अत्यन्त सशक्त तया प्रभावो- लादक बन पड़ा है। कलाकार का बदला जीवन सौन्दर्य को ही चुनौती नहीं देता, अत्याचारी को भी जैसे सूर्यहीन लोक के अतल अंधकार में हाल देता है। सहनशील विशु तया विद्रोही धर्मपद में जैसे कला के प्राचीन और नवीन युग मूर्तिमान हो उठे हैं | धर्मपद में आधुनिक कला कार का विद्रोह ही जैसे व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है। विशु और धर्मपद का पिता-पुत्र का नाता और तत्संबंधी करुण-कथा जैसे इतिहास के गर्जन में मानव हृदय की धड़कन भी घुल-मिल कर नाटक को मामि- कता प्रदान करती है। आज के राजनीतिक-आयिक संघर्ष के जर्जर युग में कोणार्क के द्वारा कला और संस्कृति जैसे अपनी चिरंतन उपेक्षा का विद्रोहपूर्ण संदेश मनुष्य के पास पहुंचा रही हैं।"
प्रमुख पात्र-
सूत्रधारः उपक्रम, उपसंहार और उपकथनों के वृन्दवार्तिक
विशु: उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता
धर्मपद: एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी
नरसिंहदेव :उत्कल-नरेशराज
चालुक्य: उत्कल-नरेश का महामात्य
सौम्य श्री दत्त: विशु का मित्र और मन्दिर का नाट्याचार्य
राजीव :मुख्य पाषाण-कोर्तक शैवालिक चालुक्य का दूत
महेन्द्रवर्मन: नरसिंह देव का रहस्याधिकारी
भास्कर गजाधर, अन्य शिल्पी प्रतिहारीगण, सैनिक, पहली याचिका, दूसरी याचिका
कोणार्क का कथानक तीन अंकों में विभाजित है-
प्रथम अंक-
प्रथम अंक में महाशिल्पी विशु का मंदिर के शिखर के ठीक से नही जम पाने के लिये चिंतन का चित्रण किया गया है। मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। केवल शिखर की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। समस्या है-यहाँ पुराने शिल्पी और उसके अप्रतिष्ठित नए उत्तराधिकारी की। इस अंक में कोणार्क मंदिर के एक कक्ष में महाशिल्पी विशु को मंदिर के मुख्य भाग विमान की रचना के लिए चिंतातुर दिखाया गया है। मंदिर सर्वांग सुंदर बना है, परंतु उसका ऊपरी भाग शिखर ठीक से नहीं जम पा रहा है। विशु की इस चिंता व द्वंद्व को दूर करने में उसका पुत्र धर्मपद सहायक बनता है।
द्वितीय अंक'-
लेखक ने इस अंक में उसी कक्ष में घटित घटनाओं को दिखलाया है। उत्कल नरेश द्वारा विशु को दिए गए सम्मान को विशु धर्मपद को अनुशंसित करते हैं। उत्कल नरेश कोणार्क मंदिर के स्थापत्य की प्रशंसा करते हैं तथा महाशिल्पी विशु को सम्मान स्वरूप रत्नमाला प्रदान करते हैं, जिसका सच्चा अधिकारी विशु धर्मपद को बताता है। उसके अनुरोध पर महाशिल्पी पद का सम्मानजनक पद धर्मपद को दिया जाता है। नरसिंह के समक्ष महामात्य राजराज के अत्याचारों की लोमहर्षक कथा आती है। इसी स्थान पर महाराज को महामात्य चालुक्य राजराज के विद्रोह और आक्रमण की सूचना भी प्राप्त होती है। कोणार्क की रक्षा का वचन धर्मपद महाराज को देकर उन्हें यहाँ के दायित्व से चिंतामुक्त करता है।
तृतीय अंक'-
तीसरा अंक संघर्षपूर्ण परिस्थितयों से भरा पड़ा है, जिसमें सभी पात्र विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए निकलते हैं। अपने पुत्र की रक्षा के लिए अधीर व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त विशु का द्वंद्वपूर्ण होना उसके पश्चाताप का चरमोत्कर्ष है। अंततः बहुत प्रयत्न करने पर भी वह धर्मपद की रक्षा करने में असमर्थ होता है। धर्मपद युद्ध करते हुए शत्रु के हाथों बहुत ही भयावह मृत्यु को प्राप्त होता है। अंत में राजराज के मंदिर में घुसने की चेष्टा को निष्फल करने के लिए विशु शिखर भाग को ध्वस्त कर देता है। राजराज और सैनिकों की मृत्यु के पश्चात वह भी प्राणोत्सर्ग कर धर्मपद के पास चला जाता है। इस प्रकार तृतीय अंक' बहुत ही मार्मिक व त्रासदपूर्ण घटनाओं और विषम स्थितियों से गुज़र कर समाप्त होता है।
कोणार्क नाटक का उद्देश्य -
'कोणार्क' नाटक के माध्यम से नाटककार का उद्देश्य 'कलावाद की समस्या एवं समाधान' स्पष्ट प्रकट हो रहा है। नाटककार अपने नाटक के माध्यम से महाशिल्पी और अन्य शिल्पियों के संघर्ष और द्वंद्व को पूरी
*द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं*
आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव (सन् 1903 से 1916) को द्विवेदी-युग के नाम से जाना जाता है। डॉ नगेन्द्र ने द्विवेदी युग को 'जागरण-सुधार काल' भी कहा जाता है और इसकी समयावधि 1900 से 1918 ई. तक माना। वहीं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को 'नई धारा: द्वितीय उत्थान' के अन्तर्गत रखा है तथा समयावधि सन् 1893 से 1918 ई. तक माना है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है।
इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इन्होने " सरस्वती " पत्रिका का सम्पादन किया। इस पत्रिका मे ऐसे लेखों का प्रकाशन किया, जिसमे नवजागरण का संदेश जन-जन तक पहुँचाया गया। इस पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। द्विवेदी मंडल के कवियों में मैथलीशरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', गोपालशरण सिंह, लोचन प्रसाद पाण्डेय और महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा 'शंकर' और राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' आदि हैं।
द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं
इस प्रकार है--
*भावगत विशेषताएँ**
1 *. देशभक्ति एवं राष्ट्रीय चेतना-*
द्विवेदी युग मे देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल मे देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएँ लिखी गई।दूसरी ओर कविता मे लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य मे कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया। इस युग मे ऐतिहासिकता, पौराणिकता मे भी राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय भावना का स्वर ही उभरकर सामने आता है।द्विवेदीयुगीन कवियों ने जनमानस के बीच राष्ट्रप्रेम का लहर चलाई। स्वतन्त्रता के प्रति जनमानस में चेतना का संचार किया। इस युग के रचनाकारों का राष्ट्रप्रेम भारतेन्दु युग की भाँति सामयिक रुदन से नहीं जुङा है, बल्कि समस्याओं के कारणों पर विचार करने के साथ-साथ उनके लिए समाधान ढूँढने तक जुङा है
’’हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी।
आओ मिलकर विचारें ये समस्याएँ सभी।।’’
2. *अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध*
इस काल की कविताओं मे सामाजिक अंध विश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए इसीलिए यह युग सुधारवादी युग भी कहलाता है। इस युग के कवियों ने सामाजिक समस्याओं, यथा – दहेज प्रथा, नारी उत्पीङन , छूआछूत, बाल विवाह आदि को अपनी कविता का विषय बनाया।
3. *मानव प्रेम-*
द्विवेदी युगीन कविताओं मे मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। इस काल का कवि संकीर्णताओं से ऊपर उठ गया है। वह मानव-मानव में भ्रातृ-भाव की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध है। अत: वह कहता है-
"जैन बोद्ध पारसी यहूदी,मुसलमान सिक्ख ईसाई।
कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम हैं भाई-भाई॥"
4. *प्रकृति चित्रण-*
द्विवेदी युग में प्रकृति को काव्य-विषय के रूप में पहली बार महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसके पूर्व प्रकृति या तो उद्दीपन के रूप में आती थी या फिर अप्रस्तुत विधान का अंग बनकर। वहीं इस युग में प्रकृति को आलंबन तथा प्रस्तुत विधान के रूप में मान्यता मिली। द्विवेदी युग में प्रकृति का गतिशील चित्रण न होकर स्थिर चित्रण हुआ है।
इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे है। प्रकृति का स्वतन्त्र रूप मे मनोहारी चित्रण मिलता है।द्विवेदी युग के कवि का ध्यान प्रकृति के यथा-तथ्य चित्रण की ओर गया। प्रकृति चित्रण कवि के प्रकृति-प्रेम स्वरूप विविध रूपों में प्रकट हुआ। श्रीधर पाठक,रामनरेश त्रिपाठी,हरिऔद्य तथा मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में प्रकृति आलंबन,मानवीकरण तथा उद्दीपन आदि रूपों में चित्रित किया गया है। श्रीधर पाठक ने काश्मीर की सुषमा का रमणीय वर्णन करते हुए लिखा-
"प्रकृति जहां एकांत बैठि निज रूप संवारति।
पल-पल पलटति भेष छनिक छवि छिन-छिन धारति॥"
5. *आदर्शवादिता -*
इस युग की कविता प्राचीन प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों से युक्त आदर्शवादी कविता है। इस युग के कवि की चेतना नैतिक आदर्शों को विशेष मान्यता दे रही थी,क्योंकि उन्होंने वीरगाथा काल तथा रीतिकाल की शृंगारिकता के दुष्परिणाम देखे थे। अत: वह इस प्रवृत्ति का उन्मूलन कर देश को वीर-धीर बनाना चाहता है-
"रति के पति! तू प्रेतों से बढ़कर है संदेह नहीं,
जिसके सिर पर तू चढ़ता है उसको रुचता गेह नहीं।"
इस काल का कवि सौंदर्य के प्रति उतना आकृष्ट नहीं,जितना कि वह शिव की ओर आकृष्ट है।
6. *नारी का उत्थान -*
इस काल के कवियों ने नारी के महत्त्व को समझा,उस पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया। अब नारी भी लोक-हित की आराधना करने वाली बन गई। अत: प्रिय-प्रवास की राधा कहती है-
"प्यारे जीवें जग-हित करें,गेह चाहे न आवै।" प्रतापनारायण मिश्र नारी के वैधव्य जीवन और बाल विधवाओं की तरुण अवस्थाओं को देखकर
बिहारी की भावगत एवं कलागत विशेषताएँ, बिहारी का गागर नें सागर स्वरूप। बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी *'बिहारी लाल का काव्य-सौंदर्य'*
*"सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर।
देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर।।"*
बिहारी लाल हिंदी के रीतिकाल के ऐसे अद्वितीय कवि हैं, जिन्होंने अपने दोहे की नन्ही सी गागर में भाव और अर्थ का लहराता हुआ सागर भर दिया है।
बिहारी की कविता में श्रृंगार के मादक चित्र हैं, कल्पना का मोहक सौंदर्य है, भाव की गहराई है, अलंकारों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग है।
बिहारी की एक ही प्रसिद्ध काव्य कृति है-'बिहारी सतसई' इसमें राजा जयसिंह के दरबार में रहकर लिखे गए बिहारी के 719 (कुछ विद्वान 713 मानते हैं) दोहे संग्रहित हैं।
राजदरबार में रहकर बिहारी ने वैभव विलास देखा था। कला की सूक्ष्म पकड़ और वाणी का कौशल प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति उनके दोहों में देखी जा सकती हैं।
*_बिहारी-भावपक्ष_*
*गागर में सागर भरने वाले कवि-*
'गागर में सागर भरना’ एक मुहावरा है। इसका अर्थ है- थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने की कला । कवि बिहारी ने अपनी काव्य-रचना के लिए छोटे से छंद दोहा को चुना है। दो पंक्तियों में वह इतना भाव सौन्दर्य, अलंकरण और कथन की विचित्रता भर देते हैं कि पाठक मुग्ध हो जाता है। संकलित दोहों में अनेक दोहे बिहारी के इस गुण को प्रमाणित करते हैं।
“अर्जी तरयौना… मुकुतन के संग ॥”
दोहे में कवि ने विराधोभास का चमत्कार प्रदर्शित करते हुए, अनेक विषयों को नीति-कथन का लक्ष्य बनाया है। साधारण अर्थ है कि निरंतर एक ही रंग (स्वर्ण वर्ण) में रहते हुए, तरयौना कान में ही पड़ा हुआ है, जबकि मोतियों से युक्त होकर बेसर नाक पर स्थान पा गई है। यहाँ कवि ने ‘कान’ की उपेक्षा ‘नाक’ को श्रेष्ठ-सम्मान का प्रतीक-बताया है। अन्य अर्थों में वेद-अध्ययन की अपेक्षा महापुरूषों की संगति को उद्धार का श्रेष्ठ साधन बताया गया है। इसके अतिरिक्त कवि ने राजदरबारों में व्याप्त आपसी कांट-छांट के वातावरण को भी प्रकाशित किया है। ‘श्रुति सेवन’ का अर्थ कान भरना -चुगली करना-और ‘नाकवास’ को सम्मान का स्थान बताते हुए, ‘तटस्थ और निष्पक्ष’ व्यवहार की महत्ता सिद्ध की है।
*श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी-* बिहारी श्रृंगार रस के कवि है। श्रृंगार रस के अलावा उनकी सतसई में भक्ति, नीति,ज्ञान और वैराग्य पर भी दोहे पाए जाते हैं, जिससे उनके काव्य में चार चांद लग गए हैं।
*श्रृंगार रस की प्रधानता-
अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएँ, प्रयोगवाद के जनक
मीराबाई के काव्य की विशेषताएं, मीरा की भक्ति भावना
तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएँ-भावगत एवं कलागत विशेषताएँ ,तुलसीदास का समन्वय लोकनायक रूप।
जयशंकर प्रसाद के 'आँसू' काव्य की काव्यगत विशेषताएँ-डॉ. मधुगुप्ता