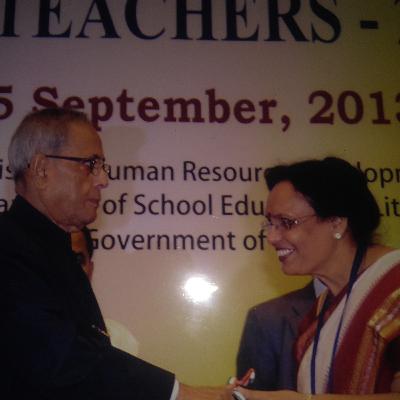कोणार्क-जगदीश चंद्र माथुर एक विहंगम दृष्टि-मधुगुप्ता
Update: 2021-03-30
Description
'कोणार्क' - जगदीश चंद्र माथुर
(एक विहंगम दृष्टि)-डॉ. मधुगुप्ता
'कोणार्क' जगदीश चन्द्र माथुर का एक प्रसिद्ध नाटक है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार "जगदीशचन्द्र माथुर का 'कोणार्क अत्यन्त सफल कृति है। नाट्यकला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि अन्यत्र देखने को नहीं मिली। विषय निर्वाचन, कथा-वस्तु, क्रम-विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्ययिता आदि दृष्टियों से कोणार्क अद्भुत कला-कृति है, जिसमें नाटक की सीमाएँ एक रहस्य विस्तार में खो-सी गई हैं। उपक्रम मेंमें आंखों के सामने एक विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंसशेप, कल्पना में समुद्र की तरह आरपार उद्वेलित होकर साकार हो उठता है, जिसकी तरंगों के व्यया-द्रवित उत्यान-पतन में करुण, विद्रोह-भरा नाटक का कयानक मन की आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाता है। उपसंहार में नाटक की अमर अमिट अनुगूंज हृदय के श्रवणों में अविराम गूंजती रहती हैं। इस नाटक का तृतीय अंक अत्यन्त सशक्त तया प्रभावो- लादक बन पड़ा है। कलाकार का बदला जीवन सौन्दर्य को ही चुनौती नहीं देता, अत्याचारी को भी जैसे सूर्यहीन लोक के अतल अंधकार में हाल देता है। सहनशील विशु तया विद्रोही धर्मपद में जैसे कला के प्राचीन और नवीन युग मूर्तिमान हो उठे हैं | धर्मपद में आधुनिक कला कार का विद्रोह ही जैसे व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है। विशु और धर्मपद का पिता-पुत्र का नाता और तत्संबंधी करुण-कथा जैसे इतिहास के गर्जन में मानव हृदय की धड़कन भी घुल-मिल कर नाटक को मामि- कता प्रदान करती है। आज के राजनीतिक-आयिक संघर्ष के जर्जर युग में कोणार्क के द्वारा कला और संस्कृति जैसे अपनी चिरंतन उपेक्षा का विद्रोहपूर्ण संदेश मनुष्य के पास पहुंचा रही हैं।"
प्रमुख पात्र-
सूत्रधारः उपक्रम, उपसंहार और उपकथनों के वृन्दवार्तिक
विशु: उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता
धर्मपद: एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी
नरसिंहदेव :उत्कल-नरेशराज
चालुक्य: उत्कल-नरेश का महामात्य
सौम्य श्री दत्त: विशु का मित्र और मन्दिर का नाट्याचार्य
राजीव :मुख्य पाषाण-कोर्तक शैवालिक चालुक्य का दूत
महेन्द्रवर्मन: नरसिंह देव का रहस्याधिकारी
भास्कर गजाधर, अन्य शिल्पी प्रतिहारीगण, सैनिक, पहली याचिका, दूसरी याचिका
कोणार्क का कथानक तीन अंकों में विभाजित है-
प्रथम अंक-
प्रथम अंक में महाशिल्पी विशु का मंदिर के शिखर के ठीक से नही जम पाने के लिये चिंतन का चित्रण किया गया है। मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। केवल शिखर की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। समस्या है-यहाँ पुराने शिल्पी और उसके अप्रतिष्ठित नए उत्तराधिकारी की। इस अंक में कोणार्क मंदिर के एक कक्ष में महाशिल्पी विशु को मंदिर के मुख्य भाग विमान की रचना के लिए चिंतातुर दिखाया गया है। मंदिर सर्वांग सुंदर बना है, परंतु उसका ऊपरी भाग शिखर ठीक से नहीं जम पा रहा है। विशु की इस चिंता व द्वंद्व को दूर करने में उसका पुत्र धर्मपद सहायक बनता है।
द्वितीय अंक'-
लेखक ने इस अंक में उसी कक्ष में घटित घटनाओं को दिखलाया है। उत्कल नरेश द्वारा विशु को दिए गए सम्मान को विशु धर्मपद को अनुशंसित करते हैं। उत्कल नरेश कोणार्क मंदिर के स्थापत्य की प्रशंसा करते हैं तथा महाशिल्पी विशु को सम्मान स्वरूप रत्नमाला प्रदान करते हैं, जिसका सच्चा अधिकारी विशु धर्मपद को बताता है। उसके अनुरोध पर महाशिल्पी पद का सम्मानजनक पद धर्मपद को दिया जाता है। नरसिंह के समक्ष महामात्य राजराज के अत्याचारों की लोमहर्षक कथा आती है। इसी स्थान पर महाराज को महामात्य चालुक्य राजराज के विद्रोह और आक्रमण की सूचना भी प्राप्त होती है। कोणार्क की रक्षा का वचन धर्मपद महाराज को देकर उन्हें यहाँ के दायित्व से चिंतामुक्त करता है।
तृतीय अंक'-
तीसरा अंक संघर्षपूर्ण परिस्थितयों से भरा पड़ा है, जिसमें सभी पात्र विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए निकलते हैं। अपने पुत्र की रक्षा के लिए अधीर व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त विशु का द्वंद्वपूर्ण होना उसके पश्चाताप का चरमोत्कर्ष है। अंततः बहुत प्रयत्न करने पर भी वह धर्मपद की रक्षा करने में असमर्थ होता है। धर्मपद युद्ध करते हुए शत्रु के हाथों बहुत ही भयावह मृत्यु को प्राप्त होता है। अंत में राजराज के मंदिर में घुसने की चेष्टा को निष्फल करने के लिए विशु शिखर भाग को ध्वस्त कर देता है। राजराज और सैनिकों की मृत्यु के पश्चात वह भी प्राणोत्सर्ग कर धर्मपद के पास चला जाता है। इस प्रकार तृतीय अंक' बहुत ही मार्मिक व त्रासदपूर्ण घटनाओं और विषम स्थितियों से गुज़र कर समाप्त होता है।
कोणार्क नाटक का उद्देश्य -
'कोणार्क' नाटक के माध्यम से नाटककार का उद्देश्य 'कलावाद की समस्या एवं समाधान' स्पष्ट प्रकट हो रहा है। नाटककार अपने नाटक के माध्यम से महाशिल्पी और अन्य शिल्पियों के संघर्ष और द्वंद्व को पूरी
(एक विहंगम दृष्टि)-डॉ. मधुगुप्ता
'कोणार्क' जगदीश चन्द्र माथुर का एक प्रसिद्ध नाटक है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार "जगदीशचन्द्र माथुर का 'कोणार्क अत्यन्त सफल कृति है। नाट्यकला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि अन्यत्र देखने को नहीं मिली। विषय निर्वाचन, कथा-वस्तु, क्रम-विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्ययिता आदि दृष्टियों से कोणार्क अद्भुत कला-कृति है, जिसमें नाटक की सीमाएँ एक रहस्य विस्तार में खो-सी गई हैं। उपक्रम मेंमें आंखों के सामने एक विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंसशेप, कल्पना में समुद्र की तरह आरपार उद्वेलित होकर साकार हो उठता है, जिसकी तरंगों के व्यया-द्रवित उत्यान-पतन में करुण, विद्रोह-भरा नाटक का कयानक मन की आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाता है। उपसंहार में नाटक की अमर अमिट अनुगूंज हृदय के श्रवणों में अविराम गूंजती रहती हैं। इस नाटक का तृतीय अंक अत्यन्त सशक्त तया प्रभावो- लादक बन पड़ा है। कलाकार का बदला जीवन सौन्दर्य को ही चुनौती नहीं देता, अत्याचारी को भी जैसे सूर्यहीन लोक के अतल अंधकार में हाल देता है। सहनशील विशु तया विद्रोही धर्मपद में जैसे कला के प्राचीन और नवीन युग मूर्तिमान हो उठे हैं | धर्मपद में आधुनिक कला कार का विद्रोह ही जैसे व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है। विशु और धर्मपद का पिता-पुत्र का नाता और तत्संबंधी करुण-कथा जैसे इतिहास के गर्जन में मानव हृदय की धड़कन भी घुल-मिल कर नाटक को मामि- कता प्रदान करती है। आज के राजनीतिक-आयिक संघर्ष के जर्जर युग में कोणार्क के द्वारा कला और संस्कृति जैसे अपनी चिरंतन उपेक्षा का विद्रोहपूर्ण संदेश मनुष्य के पास पहुंचा रही हैं।"
प्रमुख पात्र-
सूत्रधारः उपक्रम, उपसंहार और उपकथनों के वृन्दवार्तिक
विशु: उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता
धर्मपद: एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी
नरसिंहदेव :उत्कल-नरेशराज
चालुक्य: उत्कल-नरेश का महामात्य
सौम्य श्री दत्त: विशु का मित्र और मन्दिर का नाट्याचार्य
राजीव :मुख्य पाषाण-कोर्तक शैवालिक चालुक्य का दूत
महेन्द्रवर्मन: नरसिंह देव का रहस्याधिकारी
भास्कर गजाधर, अन्य शिल्पी प्रतिहारीगण, सैनिक, पहली याचिका, दूसरी याचिका
कोणार्क का कथानक तीन अंकों में विभाजित है-
प्रथम अंक-
प्रथम अंक में महाशिल्पी विशु का मंदिर के शिखर के ठीक से नही जम पाने के लिये चिंतन का चित्रण किया गया है। मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। केवल शिखर की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। समस्या है-यहाँ पुराने शिल्पी और उसके अप्रतिष्ठित नए उत्तराधिकारी की। इस अंक में कोणार्क मंदिर के एक कक्ष में महाशिल्पी विशु को मंदिर के मुख्य भाग विमान की रचना के लिए चिंतातुर दिखाया गया है। मंदिर सर्वांग सुंदर बना है, परंतु उसका ऊपरी भाग शिखर ठीक से नहीं जम पा रहा है। विशु की इस चिंता व द्वंद्व को दूर करने में उसका पुत्र धर्मपद सहायक बनता है।
द्वितीय अंक'-
लेखक ने इस अंक में उसी कक्ष में घटित घटनाओं को दिखलाया है। उत्कल नरेश द्वारा विशु को दिए गए सम्मान को विशु धर्मपद को अनुशंसित करते हैं। उत्कल नरेश कोणार्क मंदिर के स्थापत्य की प्रशंसा करते हैं तथा महाशिल्पी विशु को सम्मान स्वरूप रत्नमाला प्रदान करते हैं, जिसका सच्चा अधिकारी विशु धर्मपद को बताता है। उसके अनुरोध पर महाशिल्पी पद का सम्मानजनक पद धर्मपद को दिया जाता है। नरसिंह के समक्ष महामात्य राजराज के अत्याचारों की लोमहर्षक कथा आती है। इसी स्थान पर महाराज को महामात्य चालुक्य राजराज के विद्रोह और आक्रमण की सूचना भी प्राप्त होती है। कोणार्क की रक्षा का वचन धर्मपद महाराज को देकर उन्हें यहाँ के दायित्व से चिंतामुक्त करता है।
तृतीय अंक'-
तीसरा अंक संघर्षपूर्ण परिस्थितयों से भरा पड़ा है, जिसमें सभी पात्र विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए निकलते हैं। अपने पुत्र की रक्षा के लिए अधीर व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त विशु का द्वंद्वपूर्ण होना उसके पश्चाताप का चरमोत्कर्ष है। अंततः बहुत प्रयत्न करने पर भी वह धर्मपद की रक्षा करने में असमर्थ होता है। धर्मपद युद्ध करते हुए शत्रु के हाथों बहुत ही भयावह मृत्यु को प्राप्त होता है। अंत में राजराज के मंदिर में घुसने की चेष्टा को निष्फल करने के लिए विशु शिखर भाग को ध्वस्त कर देता है। राजराज और सैनिकों की मृत्यु के पश्चात वह भी प्राणोत्सर्ग कर धर्मपद के पास चला जाता है। इस प्रकार तृतीय अंक' बहुत ही मार्मिक व त्रासदपूर्ण घटनाओं और विषम स्थितियों से गुज़र कर समाप्त होता है।
कोणार्क नाटक का उद्देश्य -
'कोणार्क' नाटक के माध्यम से नाटककार का उद्देश्य 'कलावाद की समस्या एवं समाधान' स्पष्ट प्रकट हो रहा है। नाटककार अपने नाटक के माध्यम से महाशिल्पी और अन्य शिल्पियों के संघर्ष और द्वंद्व को पूरी
Comments
In Channel